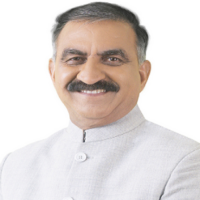यह प्रदेश में रबी की मुख्य दलहनी फसल है।



चना की खेती
भूमि
अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा रेतीली दोमट भूमि चने की खेती के लिए उत्तम है।
भूमि की तैयारी
गेहूं की तरह चने को बहुत अच्छी प्रकार तैयार किए गए खेत की जरूरत नहीं होती है। प्रायः 1-2 जुताईयां काफी होती हैं। जमीन थोड़ी भिकड़ों / ढेलों वाली होनी चाहिए ताकि जड़ों में हवा का अच्छी तरह प्रवेश हो सके।
बिजाई का समय
चने की बिजाई का सामान्य समय मध्य अक्तूबर है। इससे उखेड़ा रोग की रोकथाम हो जाती है। अगेती बिजाई से फसल में उखेडा रोग लग जाता है, क्योंकि बिजाई के समय तापमान काफी अधिक होता है और पौधों की असाधारण वृद्धि हो जाती है, जिससे उपज में काफी कमी आती है। यदि चने की गेहूं या जौं के साथ मिश्रित खेती की जाए तो बिजाई का समय गेहूं या जौं की बिजाई के साथ ही होगा।
बिजाई का ढंग
हिमाचल चना-1, हिमाचल चना 2 व जी.पी.एफ. 2 किस्मों को 30 सें.मी. की दूरी की कतारों में एवं एच.पी.जी.-17 को 50 सै.मी. की दूरी की कतारों में बीजना चाहिए। बीज को 10-12.5 सै.मी. गहरा डालना चाहिए क्योंकि कम गहरी बिजाई करने पर उखेड़ा रोग लग जाता है।
बीज की मात्रा
शुद्ध फसल के लिए |
बीज की मात्रा |
| छोटे व मध्यम दाने जैसे हिमाचल चना-2 व जी.पी.एफ.-2 | 40-45 कि.ग्रा./हैक्टेयर |
| बड़े दाने जैसे एच.पी.जी-17 | 80 कि.ग्रा./हैक्टेयर |
अनुमोदित किस्में
किस्में |
विशेषताएँ |
| हिम पालम चना-1 (डी.के.जी. 986) |
|
|
हिमाचल चना-2
|
|
|
एच.पी.जी.-17
|
|
| जी.पी.एफ.-2 |
|
जल प्रबंधन
● यदि बिजाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी हो और उसके बाद सर्दियों में 1-2 बारिशें हो जाएं तो दलहनी फसलों को सिंचाई की कोई जरूरत नहीं होती है।
● फली वाली फसलों को आरंभ मे वैसे भी पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे एक तो जड़ों में गांठे बनने में रूकावट आती है और दूसरा जड़ों को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती है।
● यदि सिंचाई की सुविधा हो तो एक सिंचाई फूल पड़ने पर तथा दूसरी सिंचाई फलियां बनने पर देनी चाहिए।
खाद व उर्वरक
तत्व (कि.ग्रा./है.) |
उर्वरक (कि.ग्रा./है.) |
उर्वरक (कि.ग्रा./बीघा) |
||||||
ना. |
फा. |
पो. |
यूरिया |
एसएसपी |
एम ओ पी |
यूरिया |
एसएसपी |
एम ओ पी |
| 30 | 60 | 30 | 65 | 375 | 50 | 5 | 30 | 4 |
पौध संरक्षण
आक्रमण / लक्षण |
रोकथाम |
1. कीट |
|
| फली छेदक: आरम्भ में सुंडियां पौधे की ऊपर की पत्तियों को खाती हैं और बाद में फलियों में छेद करके अंदर चली जाती हैं और बढ़ते हुए दानों को खाती है। |
50 प्रतिशत फूल आने पर 875 मि. ली. मोनाक्रोटोफॉस 36 एस. एल. (मोनोसिल) या 1250 ग्राम कार्बेरिल 50 डब्ल्यू.पी. (सेविन) को 625 लीटर पानी में प्रति हैक्टेयर छिडकाव करें या 50 प्रतिशत फूल आने पर अजेडिरेकटिन (0.03%) का छिड़काव करें, यदि कीड़े का प्रकोप फिर भी हो तो 45 दिन के वाद फिर छिड़काव करें। सावधानी : हरी फलियों को दवाई छिड़कने के 45 दिनों तक खाने के लिए न तोड़ें। |
| कटुआ कीट: मटमैले रंग की सुडियां भूमि में छिपी रहती हैं और उगते पौधे को भूमि की सतह से काट कर बहुत हानि पहुंचाती हैं। | दो लीटर क्लोरपाईरीफॉस 20 ई. सी. को 25 कि. ग्रा. रेत में मिलाकर प्रति हैक्टेयर बिजाई से पहले खेत में डालें। |
2. बिमारियां |
|
| झुलसा रोग: यह बिमारी गहरे काले धब्बों व छोटे-छोटे काले बिंदुओं के रूप में तने, शाखाओं, पत्तों व फलियों पर प्रकट होती है। पत्तों और फलियों पर बिमारी के लक्ष्ण एक समान दिखाई देते हैं। अधिक बिमारी होने पर पूरा पौधा ही झुलस कर मर जाता है। |
|
| उखेड़ा रोग: बिमारी वाले पौधे पहले पीले पड़ते हैं फिर मुरझा कर अंत में सूख जाते हैं। जड़ें काली हो जाती हैं और पूरी सड़ जाती हैं। |
|